Jul 6, 2011
असहमति अन्ना से हो भ्रष्टाचार से नहीं
हमारे यहाँ ऐसे बुद्धिजीवियों की कमी नहीं जो आन्दोलनों से रहते तो दूर हैं, पर सूँघने की इनकी नाक बड़ी लम्बी होती है। हर ओर इन्हें साजिश ही नजर आती है..
कौशल किशोर
आज अन्ना हजारे और उनके भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन को लेकर कई सवाल उठाये जा रहे हैं। साहित्यकार मुद्राराक्षस ने हाल ही में आरोप लगाया है कि अन्ना भाजपा व राष्ट्रीय सेवक संघ का मुखौटा हैं और अन्ना के रूप में इन्हें 'आसान झंडा'मिल गया है। जन लोकपाल समिति में ऐसे लोग शामिल हैं,जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। अन्ना हजारे की यह माँग कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में ले आया जाय, संविधान के विरुद्ध है।
मुद्राराक्षस ने यहाँ तक सवाल उठाया है कि अन्ना और उनकी सिविल सोसायटी पर संसद और संविधान की अवमानना का मुकदमा क्यों न दर्ज किया जाय? ऐसे में अन्ना हजारे और भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन की पड़ताल जरूरी है क्योंकि आज यह आन्दोलन अपने अगले चरण की ओर अग्रसर है और जन आंदोलन की शक्तियाँ वैचारिक और सांगठनिक तैयारी में जुटी हैं।
अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन ने देश की मुख्यधारा के राजनीतिक दलों को सवालों के कठघरे में खड़ा कर दिया है। हमारे संसदीय जनतंत्र में पक्ष और प्रतिपक्ष मिलकर मुख्य राजनीति का निर्माण करते हैं, लेकिन इसे विडम्बना ही कहा जायेगा कि तमाम पार्टियाँ सत्ता की राजनीतिक पार्टिर्यों में बदल गई हैं। उसके अर्थतंत्र का हिस्सा बनकर रह गई हैं aur अन्ना हजारे इसी यथार्थ की उपज हैं।
अन्ना हजारे के व्यक्तित्व और विचार में कमियाँ और कमजोरियाँ मिल सकती हैं। वे गाँधीवादी हैं। खुद गाँधीजी अपने तमाम अन्तर्विरोधों के बावजूद स्वाधीनता आन्दोलन के बड़े नेता रहे हैं। इसी तरह अन्ना हजारे के विचारों और काम करने के तरीकों में अन्तर्विरोध संभव है,लेकिन इसकी वजह से उनके आन्दोलन के महत्व को नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता है।
इस आन्दोलन का सबसे बड़ा महत्व यही है कि इनके द्वारा उठाया गया भ्रष्टाचार का मुद्दा आज केन्दीय मुद्दा बन गया है जिसने समाज के हर तबके को काफी गहरे संवेदित किया है और इसे खत्म करने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। अन्ना हजारे और उनके आंदोलन की इस उपलब्धि को क्या अनदेखा किया जा सकता है कि 42सालों से सरकार के ठंढ़े बस्ते में पड़ा लोकपाल विधेयक बाहर आया,उसे मजबूत और प्रभावकारी बनाने की चर्चा हो रही है,और इस पर सर्वदलीय बैठक आयोजित हुई।
हमारे यहाँ ऐसे बुद्धिजीवियों की कमी नहीं जो हर आन्दोलनों से रहते तो दूर हैं, पर सूँघने की इनकी नाक बड़ी लम्बी होती है। हर ओर इन्हें साजिश ही नजर आती है। ये अन्ना द्वारा नरेन्द्र मोदी की तारीफ पर तो खूब शोर मचाते हैं,लेकिन इस सम्बन्ध में अन्ना ने जो सफाई दी, ह इन्हें सुनाई नहीं देता है। किसानों की आत्म हत्या,बहुराष्ट्रीय निगमों का शोषण,चालीस करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन के लिए बाध्य किया जाना जैसे मुद्दे तो इन्हें संवेदित करते हैं लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जब प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाने की बात आती है तो वह उन्हें देश में आजादी के बाद पहली बार अल्पसंख्यक सिख समुदाय के प्रधानमंत्री को अपमानित करने का षडयंत्र नजर आता है।
अपनी बौखलाहट में ये अन्ना और सिविल सोसाइटी पर जाँच बैठा कर मुकदमा चलाने की माँग करते हैं। ये इस सच्चाई को भुला बैठते हैं कि प्रधानमंत्री किसी समुदाय विशेष का न होकर वह सरकार का प्रतिनिधि होता है। हमारे इन बौद्धिकों को अन्ना द्वारा किसान आत्महत्याओं पर भूख हड़ताल न करने पर शिकायत है लेकिन किसान आंदोलनों पर सरकार के दमन पर ये चुप्पी साध लेते हैं।
कहा जा रहा है कि अन्ना हजारे जिस लोकपाल को लाना चाहते हैं,वह संसद और सविधान की अवमानना है। पर सच्चाई क्या है ?हमारी सरकार कहती है कि यहाँ कानून का राज है। लेकिन विडम्बना यह है कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए हमारे यहाँ कोई मजबूत कानून की व्यवस्था नहीं है। मामला चाहे बोफोर्स घोटाले का हो या भोपाल गैस काँड का या पिछले दिनों के तमाम घोटालों का हो,इसने हमारे कानून की सीमाएँ उजागर कर दी हैं। तब तो एक ऐसी संस्था का होना हमारे लोकतंत्र के बने रहने के लिए जरूरी है। यह संस्था जनता का लोकपाल ही हो सकती है जिसके पास पूरा अधिकार व क्षमता हो और वह सरकार के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त व स्वतंत्र हो तथा जिसके दायरे में प्रधानमंत्री से लेकर सारे लोगों को शामिल किया जाय।
प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाने की बात को लेकर मतभेद है लेकिन अतीत में प्रधानमंत्री जैसे पद पर जब अंगुली उठती रही है तब तो यह और भी जरूरी हो जाता है। सर्वदलीय बैठक में कई दलों के प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री को इस दायरे में लाने की बात कही है और स्वयं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी उनसे मिलने गये सम्पादकों से कहा कि वे लोकपाल के दायरे में आने को तैयार हैं। फिर समस्या क्या है ?
अन्त में,भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लम्बी है। मजबूत और प्रभावकारी लोकपाल का गठन इसका पहला चरण हो सकता है। हम अन्ना हजारे से सहमत हो सकते है, असहमत हो सकते हैं या उनके विरोधी हो सकते है लेकिन यदि हम समझते है कि भ्रष्टाचार हमारे राष्ट्र,समाज,जीवन,राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति को दीमक की तरह चाट रहा है तो समय की माँग है कि इस संघर्ष को अन्ना हजारे और उनके चन्द साथियों पर न छोड़कर देश के जगरूक नागरिक,देशभक्त,बुद्धिजीवी, ईमानदार राजनीतिज्ञ लोकतांत्रिक संस्थाएँ,जन संगठन आगे आयें और इसे व्यापक जन आंदोलन का रूप दें।
जनसंस्कृति मंच लखनऊ के संयोजक और सामाजिक संघर्षों में सक्रिय.
Jul 4, 2011
राजनीतिक महत्वाकांक्षा के शिकार बाबा रामदेव
बाबा अच्छा-भला योग क्रिया के क्षेत्र में मीडिया, विशेष कर टीवी चैनल, की कृपा से देश-विदेश मेंखूब नाम पैदा करने लगे थे। नाम कमाते-कमाते उन्होंने इसी योग के क्षेत्र से 'दाम' भी खूब पैदाकिया...
तनवीर जाफरी
भारतीय राजनीति का दुर्भाग्य है कि उसमें शिक्षा-दीक्षा, पढ़ाई-लिखाई और किसी प्रकार के प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसमें तमाम ऐसे लोग भी सक्रिय हो जाते हैं जो अनपढ़ तो होते ही हैं साथ ही कई क्षेत्रों में भाग्य आज़माने के बाद भी असफल रहे होते हैं, मगर राजनीति में ऐसे लोग भी सफल होने की उम्मीद रखते हैं। इस सोच का मुख्य कारण है भारतीय राजनीति का मतों पर आधारित होना।
राजनीतिज्ञ यह जानता है कि देश में साठ से लेकर सत्तर फीसदी आबादी अशिक्षित और भोली-भाली है। इस बहुसंख्यक वर्ग को तरह-तरह के प्रलोभन, वादों, आश्वासनों तथा जाति-धर्म, वर्ग या किसी अन्य ताने-बाने में उलझा कर अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है। यह सोच भी तमाम नाकारा किस्म के लोगों को न केवलराजनीति में पर्दापण के अवसर उपलब्ध कराती है बल्कि इस प्रवृति के लोग राजनीति के क्षेत्र में कदम रखते ही बड़े-बड़े सुनहरे सपने भी सजोने लग जाते हैं। बाबा रामदेव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बाबा अच्छा-भला योग क्रिया के क्षेत्र में मीडिया विशेषकर टीवी चैनलस की कृपा से देश-विदेश में खूब नाम पैदा करने लगे थे। नाम कमाते-कमाते उन्होंने इसी योग के क्षेत्र से दाम भी खूब पैदा किया। बताया जाता है कि रामदेव इसी योग के चमत्कारस्वरूप तथा योगा जगत से सम्पर्क में आने वाले धनपतियों की दान दक्षिणा से लगभग 11 सौकरोड़ की संपत्ति के स्वामी बन चुके हैं।
एक ओर रामदेव योग के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए अपना जनाधार बढ़ाते गए, तो दूसरी ओर आम लोगों की ही तरह देश के लगभग सभी दलों के राजनेता भी रामदेव की ओर खिंच कर आने लगे। इसका कारण यह थाकि उनके योग शिविरों में आने वाले सैकड़ों लोगों से राजनेता अपनी 'हॉबी' के मुताबिक रू-ब-रू होना चाहते थे।सर्वविदित है कि हमारे देश में नेताओं का भीड़ से बहुत गहरा रिश्ता है। भीड़ को संबोधित करने, उसे अपना चेहरा दिखाने तथा उससे संवाद स्थापित करने के लिए नेता तमाम प्रकार के हथकंडे अपना सकता है। ऐसे मेंकिसी भी नेता को रामदेव के योगशिविर में जाने से आखिर क्या आपत्ति हो सकती थी, वहां तो भीड़ के दर्शनके साथ 'हेल्थ केयर टिप्स' तो बोनस में प्राप्त होने थे।
बाबा रामदेव ने भी राजनीतिज्ञों से अपने संबंधों का भरपूर लाभ उठाते हुए योग और आयुर्वेद संबंधी साम्राज्य का न केवल राष्ट्रीय, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक विस्तार किया। इसी दौरान उन्होंने धीरे-धीरे पतंजलि योगपीठ, दिव्य योग मंदिर, दिव्य फार्मेसी और आगे चलकर भारत स्वाभिमान ट्रस्ट नामक संस्थानों व संगठनों कीस्थापना कर डाली। पर लगता है कि बाबा को लगभग ग्यारह सौ करोड़ रुपये का विशाल साम्राज्य स्थापित करने के बाद भी तसल्ली नहीं हुई और उन्हें ऐसी गलतफहमी पैदा होने लगी कि क्यों न देश की राजनीति कोअपने नियंत्रण में लेकर इस देश की सत्ता पर भी नियंत्रण रखा जाए। उन्हें यह भी मुगालता होने लगा किउनका खुद का व्यक्तित्व ही कुछ निराला है, तभी तो सत्ता और विपक्ष का बड़ा से बड़ा नेता उनके योग शिविर में उनके निमंत्रण पर खिंचा चला आता है।
इस मुगालते ने धीरे-धीरे अहंकार का वह रूप धारण कर लिया, जिसने बाबा रामदेव के मुंह से अहंकार में यह तक निकलवा दिया, 'जब देश के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री मेरे चरणों में बैठते हों, फिर आखिर मैं क्यों प्रधानमंत्री बनना चाहूंगा।' इतने अहंकार भरे शब्द शायद ही अब तक देश के किसी प्रमुख व्यक्ति या साधु-संत के मुख से निकले हों। शायद योग शिविर के नाम पर लाखों लोगों को इकट्ठा करने वाले इस योगगुरु को यह भ्रम भी हो गया होगा कि जो भीड़ उन्हें विश्वविख्यात योगऋषि बना सकती है, उसी के कन्धों पर सवार होकर वे देश कीलोकतांत्रिक-राजनीतिक व्यवस्था पर भी कब्ज़ा जमा सकते हैं। हो सकता है इसीलिए बाबा रामदेव ने विदेशों सेकाला धन वापसी का मुद्दा कुछ इस अंदाज़ में उठाया गोया देश में वही अकेले ऐसे व्यक्ति हों जिन्हें विदेशों सेकाला धन वापस मंगाने की सबसे अधिक चिंता हो या देश की जनता ने उन्हें इस काम के लिए अधिकृत कर दिया हो।
दरअसल, रामदेव ने आम लोगों को भावनात्मक रूप से अपने साथ जोडऩे की गरज़ से मुद्दा तो काले धन कीवापसी का उठाया, लेकिन धीरे-धीरे वे देश में अपनी राजनीतिक शक्ति को भी तौलने लगे। पिछले संसदीय चुनावों में स्वाभिमान ट्रस्ट द्वारा शत-प्रतिशत मतदान करने की अपील के साथ पूरे देश में तमाम जगहों पर रैलियां भी निकाली गईं। यह सब कार्रवाई केवल नवगठित 'भारत स्वाभिमान संगठन' की ज़मीनी हकीकत को मापने तथा इसे प्रचारित करने के लिए की गई थी। मगर राजनीतिक तिकड़मबाजि़यों से अनभिज्ञ रामदेव कीभारतीय राजनीति के क्षितिज पर चमकने की मनोकामना आखिरकार उस समय धराशायी हो गई जब वे रामलीला मैदान से अपने समर्थकों और अनुयायियों को उनके हाल पर छोड़ कर स्वयं पुलिस से डर कर किसीमहिला के कपड़े पहनकर भाग निकले। पुलिस ने इसी हालत में उनको गिरफ्तार कार लिया।
उनकी दूसरी बड़ी किरकिरी उस समय हुई जब वे नींबू-पानी व शहद ग्रहण करने के बावजूद स्वयं को'अनशनकारी' बताते रहे। उन्हें सबसे अधिक मुंह की तब खानी पड़ी, जब इस तथाकथित अनशन को समाप्त करनेके लिए भी केंद्र सरकार का कोई प्रतिनिधि उन्हें मनाने नहीं गया। उन्होंने कुछ संतों की गुज़ारिश पर अपनीकोई मांग पूरी हुए तथा किसी सरकारी आश्वासनके बिना अनशन तोड़ दिया। अब यही बाबा रामदेव राजनीति से 'वास्तविक साक्षात्कार' होने के पश्चात काले धन की वापसी पर तो कम बोलते दिखाई दे रहे हैं, मगर अब उन्हें लोगों को यह बताना पड़ रहा है कि वे रामलीला मैदान से क्यों भागे, उन्होंने औरतों के कपड़े किन परिस्थितियों में पहने तथा अपना तथाकथित अनशन उन्हें कैसे तोडऩा पड़ा।
उनकी दूसरी बड़ी किरकिरी उस समय हुई जब वे नींबू-पानी व शहद ग्रहण करने के बावजूद स्वयं को'अनशनकारी' बताते रहे। उन्हें सबसे अधिक मुंह की तब खानी पड़ी, जब इस तथाकथित अनशन को समाप्त करनेके लिए भी केंद्र सरकार का कोई प्रतिनिधि उन्हें मनाने नहीं गया। उन्होंने कुछ संतों की गुज़ारिश पर अपनीकोई मांग पूरी हुए तथा किसी सरकारी आश्वासनके बिना अनशन तोड़ दिया। अब यही बाबा रामदेव राजनीति से 'वास्तविक साक्षात्कार' होने के पश्चात काले धन की वापसी पर तो कम बोलते दिखाई दे रहे हैं, मगर अब उन्हें लोगों को यह बताना पड़ रहा है कि वे रामलीला मैदान से क्यों भागे, उन्होंने औरतों के कपड़े किन परिस्थितियों में पहने तथा अपना तथाकथित अनशन उन्हें कैसे तोडऩा पड़ा।
अब वे अपनी धन-सपत्ति तथा तमाम आरोपित अनियमितताओं का जवाब देते फिर रहे हैं। रामलीला मैदान से उनके भेष बदल कर पलायन करने की घटना को भी संत समाज कायरतापूर्ण कार्रवाई बता रहा है जबकि बाबा रामदेव और उनके समर्थक इसे वक्त की ज़रूरत तथा सूझबूझ भरा कदम बता रहे हैं। बहरहाल बाबा रामदेव की मुश्किलें निकट भविष्य में खत्म होती दिखाई नहीं दे रही हैं। प्रत्येक आने वाला दिन उनके लिए विशेषकर उनके महत्वाकांक्षी राजनीतिक अस्तित्व के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है।
कल तक जिस अहंकार से रामदेव ने अन्ना हज़ारे के लिए यह कहा था कि-अन्ना हज़ारे पहले महाराष्ट्र तक सीमित थे उन्हें अपने मंच पर लाकर राष्ट्रीय स्तर पर मैंने उनका परिचय देशवासियों से कराया। जिस अन्ना हज़ारे के जंतर-मंतर पर आयोजित अनशन को बौना करने की गरज़ से उन्होंने अपना 'रामलीला मैदान का शो' आयोजित किया था, अब वही अन्ना अपने भविष्य के कार्यक्रम में रामदेव को अपनी शर्तों के साथ शामिल करने की बात कह रहे हैं। खबर तो यह भी है कि 16 अगस्त के अन्ना हज़ारे प्रस्तावित अनशन में रामदेव से जनता के बीच में बैठ कर अनशन में शरीक होने की बात की जा रही है, न कि मंच सांझा करने की बात। उधर प्रवर्तन निदेशालय बाबा रामदेव द्वारा इकट्ठी की गई 1100 करोड़ की संपत्ति की जांच करने में इस संदेह के कारण लग गया है कि कहीं रामदेव द्वारा फेमा नियमों का उल्लंघन तो नहीं किया गया?
कल तक जिस अहंकार से रामदेव ने अन्ना हज़ारे के लिए यह कहा था कि-अन्ना हज़ारे पहले महाराष्ट्र तक सीमित थे उन्हें अपने मंच पर लाकर राष्ट्रीय स्तर पर मैंने उनका परिचय देशवासियों से कराया। जिस अन्ना हज़ारे के जंतर-मंतर पर आयोजित अनशन को बौना करने की गरज़ से उन्होंने अपना 'रामलीला मैदान का शो' आयोजित किया था, अब वही अन्ना अपने भविष्य के कार्यक्रम में रामदेव को अपनी शर्तों के साथ शामिल करने की बात कह रहे हैं। खबर तो यह भी है कि 16 अगस्त के अन्ना हज़ारे प्रस्तावित अनशन में रामदेव से जनता के बीच में बैठ कर अनशन में शरीक होने की बात की जा रही है, न कि मंच सांझा करने की बात। उधर प्रवर्तन निदेशालय बाबा रामदेव द्वारा इकट्ठी की गई 1100 करोड़ की संपत्ति की जांच करने में इस संदेह के कारण लग गया है कि कहीं रामदेव द्वारा फेमा नियमों का उल्लंघन तो नहीं किया गया?
रामदेव के परम सहयोगी बालकृष्ण पर दो पासपार्ट रखने तथा इन पासपोर्ट पर कई विदेशी यात्राएं करने जैसे आरोप लग रहे हैं। कुल मिला कर हम यह कह सकते हैं कि बाबा रामदेव को योग ने तो आसमान पर चढ़ा दिया लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा उन्हें ले डूबी।
Jul 3, 2011
जनतंत्र भ्रम फैलाने का शासन है
आज तो जनतंत्र जनता में भ्रम पैदा करने वाला शासन है जो धूर्तता और पाखण्ड के सहारे चलता है। जनता में अपना विश्वास जमाने, भ्रम पैदा करने तथा उसे अपने पक्ष में करने के लिए शासक दल, उनकी सरकारें जनता के हाव-भाव, जीवन शैली, जनता के नारे और मुद्दे अपना लेते हैं...
कौशल किशोर
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यह कहकर कि वे लोकपाल के दायरे में आने को तैयार हैं, अन्ना हजारे की माँग का ही नैतिक समर्थन किया है। भले ही यह मनमोहन सिंह के निजी विचार हैं और इसका सरकार के दृष्टिकोण पर ज्यादा असर न पड़े । फिर भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश के प्रधानमंत्री के विचार हैं और जिन मुद्दों को लेकर सरकार और अन्ना हजारे के नागरिक समाज के बीच गतिरोध बना हुआ है, उनमें यह प्रमुख है। ऐसे में प्रधानमंत्री के इस कथन को क्या भावुकता में कही बातें समझी जाय या इसका कोई गंभीर निहितार्थ है ? इसे किस रूप में लिया जाय ?
हाल की घटनाओं ने जिन तथ्यों को उजागर किया है, उसे लेकर आम नागरिक काफी संवेदित है। आमतौर पर कहा जा रहा है कि मौजूदा तंत्र व व्यवस्था भ्रष्ट हो चुकी है। यह सरकार स्वयं कई घोटालों में फँसी है। उसके कई मंत्रियों को इन मामलों में जेल के सीखचों के पीछे जाना पड़ा है। भ्रष्टाचार से संघर्ष करने में सरकार द्वारा जो प्रतिबद्धता दिखाई जानी थी, इस सम्बन्ध में वह कमजोर साबित हुई है तथा लोकपाल बिल लाने के लिए भी वह तब तैयार हुई जब नागरिक समाज के आंदोलन का दबाव बना। और अब वह ऐसा लोकपाल लाना चाहती है जो नख दंत विहीन हो। आज ऐसी बातें आम चर्चा में हैं। इसने सरकार, कांग्रेस पार्टी तथा मंत्रियों की छवि को धूमिल किया है।
इस सबके बावजूद इस सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व के बारे में अलग राय व्यक्त की जा रही है। इनके बारे में यही कहा जाता है कि वे स्वच्छ और ईमानदार छवि वाले एक अच्छे इन्सान है। वे कमजोर हो सकते हैं। उनका लोगों से संवाद कम हो सकता है, लेकिन उनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता है। अर्थात भले ही सरकार के पाप का घड़ा भर गया हो, लेकिन उसका मुखिया पाक साफ है। सरकार, सत्ता प्रतिष्ठान, कांग्रेस पार्टी, मीडिया, राजनेताओं और बौद्धिकों के बड़े हिस्से द्वारा इसे अवधारणा के स्तर पर प्रचारित और स्थापित किया गया है।
आखिरकार राजनीति की इस परिघटना को किस रूप में देखा जाय ? अगर यह मौजूदा राजनीति की विसंगति है, तो इसकी व्याख्या कैसे की जाय ? मनमोहन सिंह एक ईमानदार व्यक्ति हैं और स्वयं इस विचार के हैं कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में आना चाहिए, तो क्या यह कुर्सी मोह या मात्र सत्ता का मोह है जो उन्हें कथित 'भ्रष्टाचार और घोटालों की सरकार' का मुखिया बने रहने के लिए बाध्य किये हुए है ? उनकी अपनी नैतिकता क्या कठघरे में नहीं खड़ी है ?
बातें तो इससे भी आगे जाकर कही जा रही हैं कि मनमोहन सिंह की सरकार कठपुतली सरकार है और इसका रिमोट कन्ट्रोल दस जनपथ के पास है। इस सरकार में निर्णय लेने की इच्छा शक्ति नहीं है और मनमोहन सिंह कांग्रेस का असली चेहरा नहीं है। इस सबके बावजूद मनमोहन सिंह अपने दल और सरकार में सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करते हैं। सत्ताधारी दल की इसके पीछे क्या मजबूरी हो सकती है ?
जहाँ तक सत्ता मोह या कुर्सी मोह की बात है, यह कहना इस विसंगति की सरलीकृत व्याख्या होगी। हकीकत तो यह है कि आज हमारी व्यवस्था राजनीतिक संकटों में फँसी है। सरकार ने जिन अमीरपरस्त नीतियों पर अमल किया है, उनसे अमीरी और गरीबी के बीच की खाई चौड़ी हुई है। सत्ता और सम्पति से बेदखल गरीबों का कोई पुरसाहाल नहीं है। वे लोग जिनके श्रम से देश चलता है, अपने हक और अधिकार से वंचित किये जा रहे हैं। महँगाई और भ्रष्टाचार से हर तबका त्रस्त है। जनता के पास आज इतनी समस्याएँ है कि वह इसके बोझ के नीचे दब सी गई है। जितनी जटिल समस्याएँ हैं, उतने ही तरह के आन्दोलन भी उठ खड़े हुए हैं।
यह सरकार के लिए कठिन स्थिति है कि उसे एक तरफ अपनी नीतियों व एजेण्डे को अमल में लाना है, वहीं उसे इसका भी ख्याल रखना है कि उसकी विश्वसनीयता जनता के बीच कायम रहे। हमारी राजनीतिक प्रणाली संसदीय जनतांत्रिक है। इसकी यही खूबी है कि जिन मतदाताओं के बूते राजनीतिक पार्टी सरकार बनाती है, उसी के ऊपर उसे शासन करना होता है और आगे शासन में बने रहने के लिए उसे उन्हीं मतदाताओं के पास जाना होता है। संकट उस वक्त आता है, जब सरकार की घोषित नीतियाँ तो कुछ और होती हैं, पर अघोषित नीतियाँ कुछ और हैं जिन पर वह अमल करती है। ऐसे में इस राजनीतिक प्रणाली की वजह से सत्ताधारी दलों और उनकी सरकार को दोहरे दबाव में काम करना होता है। यही उनके चरित्र में भी दोहरापन लाता है।
इब्राहिम लिंकन ने जनतंत्र को परिभाषित करते हुए कहा था कि यह जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। लेकिन आज के राजनीतिक संकट के युग में यह परिभाषा बहुत प्रासंगिक नहीं रह गई है। बल्कि आज तो जनतंत्र जनता में भ्रम पैदा करने वाला शासन है जो धूर्तता और पाखण्ड के सहारे चलता है। जनता में अपना विश्वास जमाने, भ्रम पैदा करने तथा उसे अपने पक्ष में करने के लिए शासक दल, उनकी सरकारें जनता के हाव-भाव, जीवन शैली, जनता के नारे और मुद्दे अपना लेते हैं। जनतंत्र में शासक वर्ग के लिए यह जरूरी होता है क्योंकि अपनी इन्हीं तरकीबों से वह अपनी सत्ता को स्थिर करता है तथा अपनी वास्तविक नीतियों को बेरोकटोक लागू करने में सफल हो पाता है।
इंदिरा गांधी इस राजनीति की कुशल खिलाड़ी थी। उन्होंने 'गरीबी हटाओ, समाजवाद लाओ' के नारे के साथ देश को तानाशाही का 'तोहफा' दिया था। बाद के सत्ताधारी दलों और उनकी सरकारों ने इसी तरह के भ्रम पर अमल किया है। आज जब मनमोहन सिंह अपने को लोकपाल के दायरे में लाने की बात करते है तो वे उसी भ्रम को फैला रहे होते हैं तथा इसका मकसद भ्रष्टाचार को लेकर जनता में उभर रहे जन असंतोष को अपने में समायोजित कर लेना है।
जनसंस्कृति मंच लखनऊ के संयोजक और सामाजिक संघर्षों में सक्रिय.
उन दीवारों का शोर किसी ने सुना नहीं...
चारों ओर से आलीशान इमारतों से घिरे उस घर की बात ही कुछ अलग थी। उसके आसपास के सभी घर दोबारा बनाए जा चुके थे। वहां सिर्फ वही एक घर था, जो मध्यमवर्गीय परिवार की झलक दिखलाता था। शायद अब तक उस घर में बड़ा फेरबदल नहीं किया गया था...
इमरान खान
 |
| बक्शे पर खूबसूरत अंदाज़ में दर्ज के-25 और अमृता प्रीतम |
दीवारें चीखती रहीं,चिल्लाती रहीं पर किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया। उस घर की एक-एक ईंट पर इतिहास के लाखों लफ्ज उभरे थे, लेकिन वो उन मजदूरों को दिखाई नहीं दिए, जो शायद पढऩा-लिखना नहीं जानते थे। उनके हर वार पर उस घर का जर्रा-जर्रा रोया तो जरूर होगा। अफसोस इतना कुछ होने पर भी किसी ने कुछ सुना नहीं, किसी ने कुछ देखा नहीं।
यह सब शायद दिल्ली में ही मुमकिन है। पंजाब की बेटी जिसने अपनी कलम से दुनिया को रौशनी दिखाते हुए औरत के हक की आवाज बुलंद की, उसका घर टूट चुका है। घर टूटते ही उसका वो सपना भी चूर-चूर हो चुका है, जिसमें उसने उस घर को सदियों तक वैसा ही रखने का सोचा था। दिल्ली के हौजखास स्थित के-25 जहां अमृता ने अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा बिताया था, वो घर अब रहा नहीं। उस घर में अमृता का परिवार जिसमें उनके दोनों बेटे, उनकी बीवियां और बच्चे रहते थे, अब वहां वीरानी छाई है।
उस घर में वो इंसान भी रहता था जो अमृता के बेहद करीब था, जिसने उसकी हर याद को संजोकर रखा था। जी हां, मैं इमरोज की ही बात कर रहा हूं। वो घर किन कारणों से बिका, इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। उनके बच्चों ने इमरोज के रहने का इंतजाम तो कर दिया है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ इससे पर्दा उठना अभी बाकी है। ज्यादातर संभावनाएं खराब आर्थिक स्थिति की हैं। अमृता तो अपनी कविताओं में रहती दुनिया तक जिंदा रहेगी, लेकिन उनके सपनों के घर को तोड़ दिया जाना भी बेहद दुखदाई है।
चारों ओर से आलीशान इमारतों से घिरे उस घर की बात ही कुछ अलग थी। उसके आसपास के सभी घर दोबारा बनाए जा चुके थे। वहां सिर्फ वही एक घर था, जो मध्यमवर्गीय परिवार की झलक दिखलाता था। शायद अब तक उस घर में बड़ा फेरबदल नहीं किया गया था, इसलिए उस घर की नक्काशी उधर से गुजरते हुए राहगीर का ध्यान अपनी ओर खींच ही लेती थी।
घर का दरवाजा शायद उस मोहल्ले के सभी दरवाजों से छोटा था। छोटा होने पर भी उसकी शान में कोई कमी मालूम नहीं पड़ती थी। दरवाजा घर की बाईं ओर था। दरवाजे के दाईं ओर गहरे जामुनी रंग के बने दो बक्सों में एक पर के-25 और दूसरे पर दर्ज था अमृता प्रीतम। दोनों बक्सों पर लटकती पत्तियां उस नाम को और भी खूबसूरत बनाती थीं। दरवाजे की दाईं ओर बेतरतीबी से उगे रंग-बिरंगे फूलों की महक एकबारगी में ही अमृता के जीवन को उसके अंतर्मन से महसूस करने वाले के जेहन में उतार देती थी।
सफेद रंग से रंगा अमृता प्रीतम का वो घर देखने वाले को एक सुकून का अहसास करवाता था, जो शायद दिल्ली में ढूंढने पर ही कहीं मिले। दरवाजे से सीधे जाने पर दाईं ओर एक छोटा दरवाजा ऊपर को जाता था, ऊपर के कमरों में ही अमृता और इमरोज ने लगभग 40 साल बिताए थे। इतनी बड़ी लेखिका का घर इतना साधारण, पहली बार वहां जाने वाला शख्स सोचता तो जरूर होगा, लेकिन दीवारों से निकलते मोहब्बत के झोंके उसे इतना मदहोश कर देते कि और कुछ सोचने की किसी में हिम्मत न रहती। घर के आखिर में पहुंचने पर वहां प्लास्टिक की एक कुर्सी और एक छोटा टेबल रखा था। छत पर टंगा पंखा भी 30-35 साल पुराना ही मालूम होता था। इमरोज अपने चाहने वालों से उसी जगह मिला करते थे।
घर टूटने का गम अमृता और इमरोज को चाहने वाले करोड़ों लोगों को होगा, पर अफसोस कि अब कुछ किया नहीं जा सकता। हमारे बहुत से दोस्त इसका साहित्यिक विरोध भी कर रहे हैं, मगर अब इसका क्या फायदा। खरीदने वाले ने तो वहां नई इमारत बनाने का काम भी शुरू करवा दिया है। विरासत का किला तो अब ढह चुका है। अब तक तो उस घर के कण-कम में बसी मोहब्बत करोड़ों लोगों के जेहन में उतर चुकी होगी।
लेखक पत्रकार हैं.
...फिर से वृक्षारोपण
आज वृक्ष लगाना सोशल वर्क की श्रेणी में सबसे नवीनतम फैशन का रूप धारण कर चुका है। विदेशी वीआईपी से लेकर देश का हर बड़ा आदमी अपने आपको पर्यावरण प्रेमी दिखाने की होड़ और दौड़ में पीछे रहना नहीं चाहता है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति हो या फिर कोई लोकल वीआईपी, सभी पेड़ लगाकर सुर्खियां बटोरने का अवसर कभी छोड़ते नहीं हैं...
डॉ. आशीष वशिष्ठ
अब के बरस सावन में... गीत के बोल रिमझिम फुहार और प्यार की बौछार की बरबस ही याद दिलाते हैं। ऐसा नहीं है कि सावन के महीने की प्रतीक्षा केवल प्रेमी-प्रेमिका ही करते हैं, बल्कि वन विभाग और एनजीओ भी इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। मानसून आते ही केन्द्र और राज्यों में वन विभाग और पर्यावरण से जुड़ी अनेक संस्थाएं एक साथ सक्रिय हो जाती हैं। सरकारी अमले के अलावा स्वयं सेवी संस्थाएं (एनजीओ) भी सुप्तावस्था से निकलकर 'एक्टिव' भूमिका में दिखाई देने लगती हैं।
सावन के महीने में पूरे देश में सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर वृक्षारोपण का जो उफान दिखाई देता है, सावन खत्म होने के साथ ही वो सारी सक्रियता ऐसे गायब हो जाती है जैसे गधे के सिर से सींग। समस्या इस बात को लेकर नहीं है कि हर साल सावन में वृक्षारोपण की रस्म अदा की जाती है, नाराजगी का कारण यह है कि एक बार पौधा लगाने के बाद उसी देखरेख और उसको संभालने की जिम्मेदारी उठाता कोई नजर नहीं आता।
सरकार और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा देशभर में लाखों वृक्षों को लगाया तो जाता है, लेकिन तस्वीर का काला पक्ष यह है कि अगला सावन तो क्या एक-दो महीनों में ही लगभग अस्सी से नब्बे फीसदी तक पौधे मुरझाकर खत्म हो जाते हैं। बेशर्मी का आलम यह है कि पर्यावरण संरक्षण और धरती को हरा-भरा बनाने की कवायद में जुटे तथाकथित नेता, पर्यावरणविद्, सामाजिक कार्यकर्ता और संस्थाएं अगले सावन में पुनः पुरानी जगह पर नया पौधा लगाकर अपनी फोटो खिंचवाते और अखबार में लंबी-चौड़ी खबरें छपवाते हैं। सरकारी स्तर पर प्रत्येक वर्ष वृक्षारोपण के लिए जितना बजट पास होता है अगर ईमानदारी से उसका दस फीसदी भी खर्च किया जाये तो देश में हरियाली का संकट आने वाले दो-तीन सालों में लगभग खत्म हो जाएगा।
वर्ष 2007 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ही दिन में प्रदेशभर में 1 करोड़ पौधे लगाकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया था। आज लगभग चार सालों के बाद उन एक करोड़ पौधों में से बामुश्किल एक लाख पौधे भी शायद ही जीवित हों। हमारे देश में पर्यावरण और उससे जुड़ी समस्याओं को न तो सरकार और न ही नागरिक गंभीरता से लेते हैं। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण और सुधारने के लिए जो भी कवायद की जाती है वो महज 'पब्लिसिटी स्टंट' और 'कागजी कार्रवाई' तक सिमट जाती है। और फिर हर साल सावन आने पर कुकरमुत्ते की भांति सैंकड़ों सामाजिक संस्थाएं और बरसाती मेंढक रूपी सरकारी तंत्र देश की गली-गली में वृक्षारोपण के गीत टर्राने लगते हैं।
देश के हर छोटे-बड़े राज्य में वन विभाग हर साल बरसात के मौसम में वृक्षारोपण के लिए भारी-भरकम बजट की व्यवस्था करता है और जिलेवार सभी वन अधिकारियों और कर्मचारियों को वृक्षारोपण का 'टारगेट' दिया जाता है। असली खेल यहीं से शुरू हो जाता है। पौध खरीदने से लेकर वृक्ष रोपने और ट्री-गार्ड लगाने तक सरकारी मशीनरी लाखों-करोड़ों का वारा-न्यारा कर चुकी होती है। हड्डी पर बचा-खुचा मांस एनजीओ और पर्यावरण को समर्पित संस्थाएं नोंच लेती हैं।
वृक्षारोपण की आड़ में जो काली कमाई की कहानी है उसमें बड़े-बड़े सफेदपोश शामिल हैं। हरियाणा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत वन विभाग ने करोड़ों के बजट से वृक्षारोपण पिछले दो-तीन सालों में करवाया, लेकिन जब एक ईमानदार वन अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने विभाग के कारनामों का कच्चा-चिट्ठा खोलना शुरू किया तो वन मंत्री से लेकर आला अधिकारी तक इस ईमानदार अधिकारी के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। इसी का नतीजा है कि पांच साल की नौकरी में नौ बार तबादला और अन्ततः निलबंन की मार संजीव को झेलनी पड़ी।
हर साल की भांति इस मानसून में भी करोड़ों पौधे रोंपे जाएंगे, लेकिन सावन बीत जाने के बाद अगर तथाकथित जिम्मेदार संस्थाओं और सरकारी मशीनरी से जिंदा पौधों का हिसाब मांगा जाए तो ऐसे-ऐसे बहाने बनाए जाएंगे कि आप चौंक जाएंगे। कहने को तो चाहे कोई कितनी लंबी चौड़ी बातें करे या बयानबाजी करे लेकिन जब जिम्मेदारी लेने का समया आता है तो स्वयं को जिम्मेदार बताने वाले दूसरों के कंधों पर जिम्मेदारी का टोकरा डालने की कोशिश करते नजर आते हैं।
धरती पर दिखाई दे रहे हैं। कुदरत ने वनों के विस्तार का अपना ही सिस्टम बना रखा है। जीव-जंतु, वनों में विचरनेवृक्षारोपण और धरती को हरा-भरा बनाने के पीछे चंद ईमानदार और निःस्वार्थी प्रयासों की बदौलत ही बचे-खुचे पौधे वाले प्राणी, पषु-पक्षी, बरसात और वन का अंदरूनी तंत्र स्वयं वनों का विस्तार करता रहता है। अगर कोई सरकार या संस्था ये दावा करती है कि उसने वनों को बनाया और लगाया है तो वो सरासर झूठ बोलती है। हां, थोड़े-बहुत क्षेत्र को वन क्षेत्र के रूप में मानव प्रयासों से विकसित किया जाता है, लेकिन दुनियाभर के जितने भी छोटे-बड़े और घने जंगल हैं उन्हें स्वयं कुदरत ने ही सजाया और संवारा है।
देश के महानगरों और नगरों में सड़कें चौड़ी करने के नाम पर हर साल लाखों वृक्षों की बलि ली जाती है। पिछले एक दशक में विकास के नाम पर करोड़ों वृक्ष देशभर में काटे गये हैं। लखनऊ में लगभग सभी प्रमुख मार्गों के विस्तार और चौड़ीकरण के नाम पर सौ-सौ साल पुराने इमली, पीपल, बरगद, गूलर आदि के हजारों पेड़ों को बेरहमी से काट डाल गया। लखनऊ शहर की जो सड़कें किसी जमाने में 'ठण्डी सड़क' के नाम से जानी जाती थी आज उन्हीं सड़कों पर गर्मी और तपिश के कारण आम आदमी का चलना दुश्वार हो चुका है।
पिछले साल दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी के नाम पर न जाने कितनेवृक्षों की बेरहम कटाई की गई। लखनऊ और दिल्ली की तर्ज पर देश के हर छोटे-बड़े कस्बे से लेकर महानगर तक विकास का पहला ठीकरा पर्यावरण पर ही फूटता है। अनियोजित विकास की जो रूपरेखा बड़ी तेजी से खींची जा रही है उसने पर्यावरण के हालात असामान्य बना दिये हैं। लखनऊ, दिल्ली, मुम्बई, मद्रास, बंगलुरू, कोलकाता, चंडीगढ, पटना, रांची में स्लम एरिया बढ़ता जा रहा है। अनियत्रिंत आबादी और शहरीकरण का बढ़ता विस्तार पर्यावरण के लिए अत्यधिक जहरीले तत्व साबित हो रहे हैं।
ऐसा भी नहीं है कि केवल सावन के मौसम में ही देश में वृक्षारोपण किया जाता है। आज वृक्ष लगाना सोशल वर्क की श्रेणी में सबसे नवीनतम फैशन का रूप धारण कर चुका है। विदेशी वीआईपी से लेकर देश का हर बड़ा आदमी अपने आपको पर्यावरण प्रेमी दिखाने की होड़ और दौड़ में पीछे रहना नहीं चाहता है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति हो या फिर कोई लोकल वीआईपी, सभी पेड़ लगाकर सुर्खियां बटोरने का अवसर कभी छोड़ते नहीं हैं।
पुराने जमाने में पेड़-पौधे लोगों की जिन्दगी का एक अहम हिस्सा थे। जन साधारण प्रकृति प्रदत्त इस अनमोल विरासत को सहेजकर रखने में विश्वास करते थे। अनेक सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में वृक्षों की उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती थी। घरों में तुलसी एवं पीपल का पौधा लगाना वृक्षों की उपयोगिता का प्रमाण था। विवाह मंडप को केले के पत्तों से सजाना, नवजात शिशु के जन्म पर घर के मुख्य द्वार पर नीम की टहनियाँ लगाना, हवन में आम की लकड़ियों का प्रयोग आदि ढेरो ऐसे उदाहरण हैं जिनसे तत्कालीन समाज में वृक्षों की उपयोगिता का बखूबी पता चलता है।
मगर आज स्थिति इसके ठीक विपरीत है। घरों में वृक्ष लगाने का चलन लगभग दम ही तोड़ चुका है और सरकार एवं एनजीओ द्वारा हर साल सावन के मौसम में वृक्षारोपण की जो खानापूर्ति और भ्रष्टाचार का खुला खेल होता है वो लगातार पर्यावरण की सेहत को बिगाड़ रहा है। जरूरत इस बात की है कि हम सच्चे मन और कर्म से लाखों-करोड़ों पौधे के स्थान पर चाहे एक ही पौधा लगाएं, लेकिन उसकी तब तक देखभाल करें, जब तक वो अपनी जड़ों पर स्वयं खड़ा न हो जाये, क्योंकि यहां सवाल धरती को हरा-भरा बनाने का है न कि गिनती गिनाने का।
देश के आम आदमी से लेकर राष्ट्रपति तक से जुड़ी पर्यावरण, प्रदूषण और उससे जुड़ी अनेक दूसरी समस्याओं को महज खानापूर्ति न समझकर हमें पूरी संजीदगी से हर दिन और हर अवसर पर अपने आस-पास एक पौधा लगाने का पवित्र संकल्प लेना चाहिए, तभी हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए हरी-भरी धरती का उपहार दे पाएंगे।
स्वतंत्र पत्रकार और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक- सामाजिक मसलों के लेखक .
Jul 2, 2011
पहला हेम चंद्र पांडे स्मृति व्याख्यान
विष्णु शर्मा
 |
| व्याख्यान प्रस्तुत करते सुमंथो बेनर्जी, साथ में भूपेन सिंह |
पहला हेम चंद्र पांडे स्मृति व्याख्यान 2 जुलाई 2011 को गाँधी शांति प्रतिष्ठान, नई दिल्ली में संपन्न हुआ. वरिष्ठ पत्रकार सुमंथो बेनर्जी ने 'प्रोफेशनल एथिक, करियरिस्म एंड सोशियों-पोलिटिकल आब्लगैशन- कन्फ्लिक्ट कन्वर्जन्स इन इंडिया जर्नलिज़म' शीर्षक के तहत व्याख्यान प्रस्तुत किया. उन्होंने बताया कि आज पत्रकार खोज करने और अपनी पसंद की राजनीति को चुनने की कीमत चुका रहे हैं. हेम को अलग से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उन्हें एक लंबी परंपरा के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए.
इस अवसर पर कार्यक्रम के संचालक भूपेन ने कहा कि पत्रकार हेमचंद्र की शहादत को एक साल हो गया है, लेकिन उनके हत्यारों को सजा मिलेगी इसका भरोसा अब तक नहीं हो सका है. आज हम हेम के आदर्शों को याद करने के लिए जुटे हैं. यहाँ उपस्थित लोगों की मौजूदगी यह साबित करती है कि यह हत्या सत्ता के लाख प्रयासों के बावजूद गुम नहीं हो सकी है. उन्होंने आगे कहा कि सरकार हेम को माओवादी बता रही है, लेकिन तब भी क्या सरकार के पास उन्हें गोली मारने का अधिकार था? आज हमारे समाचार माध्यमों को कारपोरेट चला रहे हैं. समाचार माध्यमों उद्योग बन गए हैं और इसने सत्ता के साथ एक अनैतिक गठबंधन बना लिया है.
कार्यक्रम में विशेष अथिति राजेंद्र यादव ने कहा कि हेम को जिस तरह मारा गया, वह सत्ता के लिए नया नहीं है. बहुत पहले आपातकाल के समय ऐसा दौर आया था. तब वह बहुत थोड़े समय के लिए था, लेकिन आज यह लंबे समय से जारी है. आज हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, उनमे से कोई भी हेम हो सकता है. हम लगातार एक डर के साये में जीते हैं कि कब हमें पकड़ लिया जायेगा और हमारी मौत को मुठभेड़ करार दे दिया जायेगा. उन्होंने आगे कहा कि विचार जब सत्ता में बदलता है तो वह खतरनाक हो जाता है, क्योंकि सत्ता का स्वरूप ही दमनकारी होता है. सत्ता वर्चस्ववादी होती है.
बहुचर्चित लेखिका अरुंधती रॉय ने इस अवसर पर कहा कि हेम के साथ कामरेड आज़ाद को भी याद करना जरूरी है. हमें अपने आप से यह सवाल पूछना चाहिए कि क्यों एक साल पहले हेम और कामरेड आज़ाद की हत्या हुई? उन्हें इसलिए मारा गया था कि सरकार में शामिल कुछ लोग नहीं चाहते थे कि बातचीत के जरिये माओवाद की समस्या हल निकले. हम देख रहे हैं कि इस एक साल के अंतराल में बातचीत की कोई कोशिश नहीं की गयी है. उन्होंने कहा कि सत्ता ख़ामोशी से दमन करना चाहती है और मीडिया उनका साथ दे रहा है. अन्ना हजारे के आन्दोलन के शोर में दमन की आवाज़ को छिपाया जा रहा है.
वरिष्ठ कवि और पब्लिक एजेंडा के संपादक मंगलेश डबराल ने कहा कि आज के हालत में कोई भी चेतनावान व्यक्ति तटस्थ नहीं रह सकता और हेम ने भी ऐसा ही किया. जब तक सत्ता का दमन जारी रहेगा, हेम जैसे पत्रकार पैदा होते रहेंगे.
कवि और पत्रकार नीलाभ ने कहा कि भारत एक पुलिसिया राज्य बन चुका है. हमें जोर- शोर से आवाज़ उठानी होगी, नहीं तो बहुत देर हो जायेगी. आज भारत की जेलों में हजारों पत्रकार बंद हैं. हेम के बहाने हमें उनके बारे में भी बात करनी होगी. लेखकों को इस बारे में लगातार लिखना चाहिए. फिल्म निर्माता संजय काक ने कहा कि हमें मेनस्ट्रीम मीडिया को कोसना बंद करना चाहिए. हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं है. हमे उनका सहयोग लेना आना चाहिए.
हेम के साथ अपने जुड़ाव के बारे में बताते हुए समयांतर पत्रिका के संपादक पंकज बिष्ट ने कहा कि हेम से उन्हें हौसला अफजाई मिली. वे हमेशा चर्चा करते थे कि पत्र में क्या होना चाहिए. हेम की लड़ाई में नए लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है. इस लड़ाई में वैकल्पिक मीडिया की एक सीमा है. हमे बड़े समाचार घरानों पर दवाब बनाना चाहिए कि वे नियम से चलें. दवाब बनाना जरूरी है, नहीं तो इससे छोटे समाचार माध्यम भी प्रभावित होंगे. हमें बहुत सी बातें बड़े समाचार माध्यमों से ही पता चलती हैं. वरिष्ठ पत्रकार आनंद स्वरूप वर्मा ने कहा कि सच को सामने लाने में वैकल्पिक मीडिया की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और यह उनका कर्त्तव्य भी है. पत्रकारों के पास उनकी यूनियन होना जरूरी है. और यूनियन लोकतान्त्रिक होना चाहिए. आज जो यूनियन है. लेकिन वे सत्ता की दलाली में लगे हैं और पत्रकारों के हितों की अनदेखी कर रहे हैं.
लेखक-पत्रकार आनंद प्रधान ने कहा कि समाचार माध्यम अपने पत्रकारों को संगठित नहीं होना देना चाहते. वे उनका जबरदस्त शोषण करते हैं और जब भी सरकार उनके बारे में सोचती है तब यह कहा जाता है कि सरकार उन्हें अपने पक्ष में करना चाहती है. इस अवसर पर वरिष्ठ लेखक पंकज सिंह ने भी अपनी बात रखी.
कार्यक्रम की शुरुआत में पत्रकार हेम चंद्र पांडे पर केन्द्रित एक किताब का भी विमोचन किया गया.
क्यों चुप है सरकार
आपरेशन ग्रीनहंट के इस नेतृत्वकर्ता ने जब देश की आंतरिक सुरक्षा का कार्यभार संभाला, उसके बाद देश के भीतर ही जगह-जगह उपनिवेश दिखने लगे हैं। सेना, अर्धसेना, पुलिस, गुप्तचर, प्रशासनिक अधिकारी से लेकर निजी सुरक्षाकर्मियों का पूरा लाव-लश्कर जमीन हथियाने के अभियान का अगुआ बन गया है...
अंजनी कुमार
हर्फ ए हक दिल में खटकता है जो कांटे की तरह
आज इजहार करें और खलिश मिट जाए।।
आज इजहार करें और खलिश मिट जाए।।
न तो यह कांटा निकल रहा है और न ही खलिश मिट रही है। आज यानि 2 जुलाई को पूरा एक साल बीत गया है माओवादी प्रवक्ता आज़ाद और पत्रकार हेम चन्द्र पाण्डेय की हत्या को। इस बीच पीयूसीएल की टीम ने मानवाधिकार मामलों के वकील प्रशांत भूषण के नेतृत्व में छानबीन कर अपनी रिपोर्ट में बताया कि सीपीआई माओवादी के प्रवक्ता आजाद और पत्रकार हेमचंद्र पांडे को पकड़ कर हत्या की गई। यह रिपोर्ट आंध्र प्रदेश पुलिस और गृहमंत्री चिदंबरम के 'मुठभेड़' के दावे को झुठलाती है।
अपने सितंबर 2010 के अंक में 'आउटलुक' पत्रिका ने आजाद के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की स्वतंत्र समीक्षा को छापा था। विशेषज्ञ डाक्टरों की राय में आजाद को अत्यंत पास से सीधे कोण पर गोली मारी गई थी। पुलिस की कहानी के अनुसार आजाद आदिलाबाद के जंगल में एक ऊंची पहाड़ी पर लगभग 20 माओवादियों के साथ थे। वहां पर हुई मुठभेड़ में आजाद और हेमचंद्र पांडे मारे गए। पुलिसिया कहानी के अनुसार माओवादी ऊंची पहाड़ी (500मीटर ऊपर) पर थे और पुलिस इसके निचले हिस्से में।
पीयूसीएल और अन्य जांच रिपोर्टों में यह बताया गया है कि आसपास के गांव वालों ने उस रात गोली चलने की बात को ही सिरे से नकार दिया। एफआईआर रिपोर्ट और मीडिया द्वारा प्रसारित इस खबर के बीच भी काफी गड़बड़ी दिखती है। एफआइआर रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश पुलिस इंटेलिजेंस की खबर के आधार पर 1 जुलाई को आदिलाबाद के जंगल में जाती है और एनकाउंटर होता है। जबकि वेंकेडी पुलिस स्टेशन में 2 जुलाई को एफआईआर दर्ज होता है। इसके अनुसार 20 माओवादियों के साथ 30 मिनट तक मुठभेड़ हुई, जो रात 11 बजे से चली और अलसुबह दो लोगों के शव मिले। यह एफआइआर सुबह 9.30 बजे दर्ज होती है, जबकि चैनल इस कथित मुठभेड़ की खबर को सुबह 6 बजे से प्रसारित करने लगते हैं। इस मुठभेड़ में एक भी पुलिस वाला घायल नहीं हुआ। आंध्र प्रदेश पुलिस की इस मुठभेड़ की कहानी को स्वामी अग्निवेश और प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल 2011 को इसकी जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया। बहरहाल यह जांच जारी है।
इस पूरे प्रकरण में गृहमंत्री पी. चिदम्बरम की चुप्पी खतरनाक ढ़ंग से बनी रही। आपरेशन ग्रीनहंट के इस नेतृत्वकर्ता ने जब देश की आंतरिक सुरक्षा का कार्यभार संभाला, उसके बाद देश के भीतर ही जगह-जगह उपनिवेश दिखने लगे हैं। सेना, अर्धसेना, पुलिस, गुप्तचर, प्रशासनिक अधिकारी से लेकर निजी सुरक्षाकर्मियों का पूरा लाव-लश्कर जमीन हथियाने के अभियान का अगुआ बन गया है। अपने ही देश में अपने देश के लोगों से दरबदर होते लोगों की जमीन पर कौन काबिज हो रहा है, किसका हित सध रहा है, किसका राज स्थापित हो रहा है, ...?
आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बने सीपीआई माओवादी के साथ चिदंबरम ने वार्ता की एक कूटनीति को अख्तियार किया। सीपीआई माओवादी के प्रवक्ता आजाद ने स्वामी अग्निवेश की पहल पर इस कूटनीति पर सकारात्मक रुख अपनाया। इसके चंद दिनों बाद ही कथित मुठभेड़ की कहानी में आजाद और हेमचन्द्र की हत्या कर दी गई। चिदंबरम आंतरिक सुरक्षा और वार्ता की कूटनीति के कर्ताधर्ता होने के बावजूद इस हत्या पर और आगे किसी वार्ता की संभावना पर खतरनाक ढ़ंग से चुप रहे। कांग्रेस और पूरे विपक्ष ने भी इस हत्या और वार्ता के मुद्दे पर चुप्पी को बनाए रखा। इस चुप्पी पर बहुत से सवाल खुले और परोक्ष रूप से उठाए गए, आरोप लगाए गए लेकिन संसद में इस मुद्दे पर चुप्पी बनी रही । इस चुप्पी के बहुत से मायने हैं। चुप्पी परत दर परत खोली जा सकती है। इस चुप्पी के पीछे की राजनीतिक संकीर्णता, गजालत और क्रूर आर्थिक लोभ को भी पढ़ा जा सकता है। इस चुप्पी के पीछे चल रहे नजारों को देखा जा सकता है।
पर, मसला नागरिक समाज का भी है, जिसके सामने बोलना और चुप रह जाना वैकल्पिक हो गया है। नक्सलवादी, माओवादी के मसले पर तो यह वैकल्पिक चुप्पी खतरनाक ढंग से दिख रही है। वर्ष 1967 के बाद से उभरे इस राजनीतिक विकल्प को अब लगातार विभिन्न धाराओं और कानूनों के तहत अपराध की श्रेणी में डाला जाता रहा है। और, इस श्रेणी के तहत अब तक हजारों लोगों को मुठभेड़ में मारा जा चुका है। इस अपराध के तहत मनमानी सजा मुकर्रर की गयी। हजारों लोगों ने जेल की सलाखों के पीछे जीवन गुजार दिया। आज भी यह बड़े पैमाने पर जारी है।
वर्ष 1970 के दशक में नागरिक राजनीतिक अधिकारों को लेकर बड़ी लड़ाईयां लड़ी गयीं और जीती भी गयीं। कई सारे संगठन अस्तित्व में आए। आज भी इसकी एक क्षीड़ धारा इस तरह की लड़ाइयों में लगी हुई है। आज जितने बड़े पैमाने पर राजनीतिक नागरिक अधिकारों पर हमला बोला जा रहा है, उससे यह चुनौती कई गुना बढ़ चुकी है। ऐसे में वैकल्पिक चुप्पी और संघर्ष का रास्ता खतरनाक नतीजे की ओर ले जाएगा। आजाद और हेमचंद्र पांडे की हत्या पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप सकारात्मक है। एक सकारात्मक पहल ही दमन की पहली खिलाफत है। आजाद और हेम की हत्या के मसले पर नागरिक समाज के पहल की दरकार है।
स्वतंत्र पत्रकार व राजनीतिक-सामाजिक कार्यकर्ता.फिलहाल मजदूर आन्दोलन पर कुछ जरुरी लेखन में व्यस्त.
Jul 1, 2011
'हेम जैसे समाज में थे वैसे जीवन में'- बबीता
पिछले वर्ष 2 जुलाई को माओवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता चेरुकुरी राजकुमार उर्फ़ आजाद के साथ आंध्र प्रदेश पुलिस ने उत्तराखंड के पत्रकार हेमचन्द्र पाण्डेय उर्फ़ हेमंत पाण्डेय को फर्जी मुठभेड़ में मार डाला था. हेमचन्द्र पाण्डे की यह हत्या पुलिस ने तब की जब वे आजाद का साक्षात्कार लेने नागपुर गए थे. लेखन और संघर्ष दोनों को पत्रकारिता की बुनियाद मानने वाले हेमचन्द्र की कल 2 जुलाई को पहली पुण्यतिथि है. इस मौके पर हेम के जीवन, राजनीति और अन्य विशेष पहलुओं पर उनकी पत्नी बबीता उप्रेती से विशेष बातचीत...
 |
| हेमचन्द्र पांडे : लेखन और संघर्ष साथ-साथ |
बबीता उप्रेती से अजय प्रकाश की बातचीत
सीपीआई (माओवादी) के राष्ट्रीय प्रवक्ता आजाद और आपके पति हेमचंद्र पांडेय पिछले वर्ष 2 जुलाई को एक साथ हैदराबाद के अदिलाबाद के जंगलों में मारे गये थे। फिलहाल इस मामले में क्या प्रगति है?
सरकार से न्याय न मिलने की स्थिति में हमने मानवाधिकार मामलों के प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण के जरिये सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सारे तथ्यों को देखने के बाद सुनवाई के दौरान न्यायालय ने हेम और आजाद की हत्या में शामिल उस पूरी टीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। फिलहाल एक-डेढ़ महीने से दोनों हत्याकांडों के मामले में सीबीआई जांच चल रही है।
इस मामले में सीबीआइ जांच तो बड़ी उपलब्धि मानी जायेगी?
मैं इसे एक सामान्य जांच प्रक्रिया मानती हूं, जो अदालत के हस्तक्षेप के बाद संभव हो पायी है। रही बात सीबीआइ की तो यह एजेंसी उसी गृह मंत्रालय के अंतर्गत है, जिसने आजाद और हेम को मरवाने की साजिश रची थी। हत्या की यह साजिश तब रची गयी थी, जब आजाद सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश की मध्यस्थता में माओवादियों का पक्ष रखने की प्रक्रिया में शामिल थे और पत्रकार होने के नाते हेम आजाद का साक्षात्कार लेने नागपुर गये थे। ऐसे में सीबीआइ पर भरोसे का सवाल, मेरे लिए खुद ही एक सवाल है। हां, मैं इतना जरूर कहूँगी कि अदालत ने एक सकारात्मक भूमिका निभायी है और हमें न्याय मिलने की उम्मीद है।
हेम और आजाद के मारे जाने पर सरकार ने इसे 'मुठभेड़ में आतंकवादियों' की मौत कहा', जबकि अदालत इस पूरे मामले को एक दूसरे नजरिये से देख रही है, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच इस फर्क का आप क्या कारण मानती हैं?
आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा की गयी इन हत्याओं के बाद पिछले वर्ष दो जुलाई की सुबह से अदिलाबाद, हैदराबाद और दिल्ली से घटनाक्रमों का जो सिलसिला आना शुरू हुआ, उसी से साफ हो गया था कि हत्या करने के बाद पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ की कहानी गढ़ी है। बाद में डॉक्टरों की एक टीम ने जहर देने की भी पुष्टि कर दी, मीडिया ने भी संदेहों की तथ्यजनक पुष्टि की। संभव है अदालत ने इन बारीकियों पर गौर किया हो और इस नतीजे पर पहुंची हो.
हेम आपसे आखिरी बार कब मिले थे?
तीस जून 2010 को। उस दिन वह अपने दफ्तर से डेढ़ बजे ही आ गये थे, क्योंकि उन्हें नागपुर जाना था। मैंने उनका सारा सामान पैक किया और घर से ख़ुशी-ख़ुशी विदाई की। वे 2 जुलाई की सुबह वापस आने का वायदा कर गये थे। 2 जुलाई को उनके लिए खाना बनाकर मैं इंतजार ही कर रही थी कि उनके मारे जाने की खबर आयी। उनके लिए बनाये खाने को मैंने अभी कुछ महीने पहले फेंका है।
न्याय में आप क्या चाहती हैं?
जिन लोगों ने भी हेम को मारा है उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाये। दूसरा, इस हत्या में सिर्फ वही पुलिसवाले शामिल नहीं हैं जो मौके पर उस टीम के हिस्सा थे, बल्कि हेम और आजाद को मारने की साजिश में उच्चाधिकारी भी शामिल थे। मेरा मानना है कि माओवादियों की ओर से शान्तिवार्ता की तैयारी में शामिल आजाद और उनके साथ मारे गये मेरे पति हेम की हत्या गृह मंत्रालय की इजाजत के बगैर संभव नहीं है। नहीं तो एक तरफ आजाद शांतिवार्ता के लिए चिट्ठियों का आदान-प्रदान कर रहे थे और दूसरी तरफ पुलिस वाले ठन्डे तरीके से उनकी हत्या की फिराक में क्यों गलते। इसलिए सजा उन्हें भी होनी चाहिए जो देश में शांति के दुश्मन हैं।
हेम से बिछड़े हुए आपको कल सालभर हो चुके हैं, आपको उनकी कमी किस रूप में ज्यादा खलती है?
हेम के नहीं रहने की कमी मेरे जीवन में बहुत खलती है, जिसके बारे में मैं कम-ज्यादा नहीं बता सकती। हेम मेरे प्रेमी, पति, राजनीतिक शिक्षक और सबसे बढ़कर इंसान बहुत अच्छे थे। उस तरह के व्यक्तित्व वाले लोगों को मैं अपने आसपास बहुत कम देखती हूं। मेरी उनसे दोस्ती उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में तब हुई जब मैं बारहवीं में और वे बीए प्रथम वर्ष में थे। उस दौरान वे आइसा नाम के छात्र संगठन में सक्रिय थे और मेरे भाई विजयवर्धन उप्रेती जो अब पत्रकार हैं, वह भी आइसा के कार्यकर्ता थे। घर में आइसा के लोगों का आना-जाना लगा रहता था, उसी दौरान मेरा झुकाव हेम की तरफ हुआ और प्रेम हो गया। हेम की गंभीरता और चीजों के प्रति उनकी सहजता मुझे हमेशा उनके और करीब करती रही।
उनके साथ जीवन का यह छोटा सा सफर कैसा रहा ?
बहुत ही शानदार और खूबसूरत। उनके साथ जीये आठ साल के समय की वह खूबसूरती और जीवंतता शायद अब मेरे हिस्से न आये। हेम अद्भुत इंसान थे। कभी मेरे प्रति बहुत प्रेम का प्रदर्शन नहीं किया। किसी पार्क आदि में हम बहुत कम घूमने जा पाये, शायद दो-चार बार। मगर इंसान और इंसानियत के प्रति उनका जो प्रेम था, वह हमारी जिंदगी में रफ्तार ला देता था। वर्ष 2002 में हमारी शादी हुई और कभी लगा ही नहीं कि जिंदगी झोल खा रही है। हेम जैसे समाज में थे, वैसे जीवन में भी।
 |
| बबीता और हेम : आदर्श भी, प्यार भी |
मैं उनसे कभी -कभी कहती कि हम कभी अपने बारे में बैठकर बातें क्यों नहीं करते। फिर हमारी बात शुरू होती और थोड़ी देर में वह सामाजिक मसलों की बात बनकर रह जाती। इन सिलसिलों ने मुझे समाज के बारे में खासकर महिला अधिकारों के प्रति एक नजरिया विकसित करने में बड़ी भूमिका निभाई।
तो हेम के साथ ने आपको राजनीतिक रूप से भी समझदार बनाया?
समझदार ही नहीं, बल्कि उन्होंने मुझे राजनीति का कहहरा भी सिखाया। बारहवीं तक मुझमें कोई राजनीतिक समझदारी नहीं थी। मैं बचपन से चुलबुली थी और खेलने में लगी रहती थी। घर में राजनीतिक माहौल होने के बावजूद मेरी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं बनती। हालाँकि नेपाल में उसी वक्त माओवादी आंदोलन परचम लहराने की तरफ बढ़ रहा था और इसे लेकर हमारे घर आने वाले लड़के-लड़कियां खूब बहसें करते। तो उन बहसों में मुझे यह सुनकर अच्छा लगता कि चलो ऐसे भी दुनिया बनने की ओर है, जिसमें लोगों की बेहतरी की चिंताएं की जाती हैं। इन बातों में हेम के तर्क और समझदारी ठीक लगती,जिससे मेरा झुकाव हेम की तरफ बढ़ा और वहीं से मेरी राजनीतिक जीवन की यात्रा शुरू हुई।
तो फिर हेम का राजनीतिक सफर कहां से कहां तक चला?
वह शुरू में आइसा से जुड़े और पिथौरागढ़ पीजी कॉलेज से दो बार छात्रसंघ का चुनाव भी लड़ा। एक बार चुनाव हार गये और दूसरी बार 2001 में जब जीतने की स्थिति में थे, तब उन्होंने चुनाव लड़ने से खुद ही मना कर दिया और आइसा को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? के बारे में उन्होंने कहा था कि आइसा जो कि माले का छात्र संगठन है, वह भी चुनावों के जरिये समाज बदलने के सपने देखता है, जो कि संभव नहीं है। उनकी इस समझदारी के बनने में उस बीच किये उनके गंभीर अध्ययन और नेपाली समाज में मचे उथल-पुथल ने मदद की, जिसके बाद वह उत्तराखंड में काम करने वाले छात्र संगठन एआइपीएसएफ से जुड़े। इस संगठन से जुड़ने का कारण था चुनाव नहीं लड़ना और क्रांतिकारी तरीके से समाज बदलने की राजनीतिक पहुंच। लेकिन इस संगठन में भी वह ज्यादा समय इसलिए नहीं रह सके कि वह संगठन बात ही करता था, व्यवहार न के बराबर था। उसके बाद से वह उत्तराखंड के जल, जंगल, जमीन की लड़ाई से जुड़े और सभी जनांदोलनों में शिरकत करते हुए किसान मसलों पर गंभीरता से लिखने लगे।
हेम जिन अखबारों में लिखते थे, उनके मारे जाने के बाद उन्हीं अखबारों के संपादकों ने जो रवैया अख्तियार किया, क्या वह उचित था?
हेम नई दुनिया, दैनिक जागरण और राष्ट्रीय सहारा में लिखा करते थे। उनका अंतिम लेख 2 जुलाई (जिस दिन मरे जाते हैं ) को ही दैनिक जागरण में छपता है, लेकिन इन तीनों अखबारों में सफाइयां छपती हैं कि हेम चंद्र पांडेय नाम का कोई लेखक इनके यहां लेख नहीं लिखता है। सरकार के चरण की धूल साफ करने वाली इन सफाइयों के बाद यह संपादक शर्मिंदा नहीं होते हैं और कहते हैं कि हमें क्या पता कि हेमंत पांडे ही हेमचंद्र पांडे है। जबकि इन सफाइयों के छपने से पहले मैं पचासों बार मीडिया में बोल चुकी थी कि हेम अखबारों में हेमंत पांडे के नाम से लिखते थे। साफ है कि आज के संपादकों में एक व्यावसायिक एकता भी नहीं है, जो मौका पड़ने पर पत्रकारों के पक्ष में सरकार से टकरा सकें।
माना जाता है कि ऐसा अख़बारों ने इसलिए कहा क्योंकि हेम पर माओवादी होने का आरोप था. अगर हेम आरोपी के बजाय घोषित माओवादी होते तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती ?
यही प्रतिक्रिया होती और न्याय के लिए कोशिश का तेवर भी यही होता. माओवादी हो जाने से उस व्यक्ति विशेष का इंसानी हक़ तो नहीं छिन जाता और न्याय पाना इंसानी हक़ की बुनियाद है. अब तो सर्वोच्च अदालत भी कह चुकी है कि माओवादी विचार मानने से कोई सजा का हकदार नहीं हो जाता.
इस कठिन सफर में आप किन दोस्तों, रिश्तेदारों और सामाजिक सहयोगियों को विशेष रूप से याद करना चाहेंगी?
इस प्रश्न के जवाब में किसी का नाम लूं उससे पहले मैं साफ कर देना चाहती हूं कि हेम को जानने वाले और न जानने वाले उन सभी लोगों ने इस बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, जो समाज की बेहतरी में भरोसा करते हैं। कई सारे साथी डर भी गये, लेकिन उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। उन्हें सिर्फ सुझाव दूँगी, खड़े होइये कि वक्त साथ आने का है। इस मुश्किल समय में साथ देने वाले संगठनों में पहला नाम हैदराबाद एपीसीएलसी का है। वे साथी जो मुझे नहीं जानते, मेरी भाषा नहीं जानते और जहां दमन सर्वाधिक है, वहां के लोग जिस तरह हेम और आजाद के लिए खड़े हुए, उसका बड़ा कारण एपीसीएलसी है। क्रांतिकारी कवि वरवरा राव, आरडीएफ के जीएन साईंबाबा, मेरा भाई विजयवर्धन उप्रेती, पत्रकार भूपेन सिंह, हेम के भाई राजीव पांडे, नैनीताल समाचार के संपादक राजीव लोचन शाह समेत सैकड़ों दोस्त जिनका नाम मैं नहीं गिना पा रही हूं, सबका मुझे बिखरने से बचाने में बड़ा योगदान है।
Jun 30, 2011
अब डॉक्टर नहीं रहे भगवान
एक जुलाई को डॉक्टर्स डे पर विशेष
क्या सचमुच, बदलते परिवेश में डॉक्टर अब भगवान कहलाने के लायक नहीं रह गए हैं? क्या उन्हें मरीज की जिंदगी से नहीं, बल्कि रुपए से प्यार है़...
राजेन्द्र राठौर
भगवान के बाद धरती पर अगर कोई भगवान है तो वह है डॉक्टर। मगर पिछले कुछ वर्षों में लापरवाही की कई खबरों की वजह से यह पेशा सवालों से घिरता नजर आ रहा है। ज्यादातर डॉक्टरों ने अब सेवाभावना को त्यागकर इसे व्यापार बना लिया है। उन्हें मरीज के मरने-जीने से कोई सरोकार नहीं है। वे मरीज का ईलाज तो दूर, लाश के पोस्टमार्टम करने का भी सौदा करते हैं। उनके लिए आज पैसा ही सबकुछ हो गया है। वहीं कुछ ऐसे चिकित्सक भी है, जिन्होंने मरीजों की सेवा और उनकी जिदंगी की रक्षा को ही अपना मूल उद्देश्य बना रखा है। वे अपने इस मिशन में अकेले ही आगे बढ़ते जा रहे हैं।
इस मुद्दे पर बात इसलिए की जा रही है, क्योंकि आज यानि एक जुलाई को भारत देश में डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। दरअसल, भारत में डॉ. बीसी रॉय के चिकित्सा जगत में योगदान की स्मृति में एक जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। एक दशक पहले की बात की जाएं तो, उस समय तक डॉक्टरों को भगवान माना जाता था। धरती पर अगर कोई भगवान कहलाता था, वह डॉक्टर ही था। लोग डॉक्टर की पूजा करते थे, आखिर पूजा करते भी क्यों नहीं। डॉक्टर, जिंदगी की अंतिम सांस ले रहे व्यक्ति को फिर से स्वस्थ जो कर देते थे।
इस मुद्दे पर बात इसलिए की जा रही है, क्योंकि आज यानि एक जुलाई को भारत देश में डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। दरअसल, भारत में डॉ. बीसी रॉय के चिकित्सा जगत में योगदान की स्मृति में एक जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। एक दशक पहले की बात की जाएं तो, उस समय तक डॉक्टरों को भगवान माना जाता था। धरती पर अगर कोई भगवान कहलाता था, वह डॉक्टर ही था। लोग डॉक्टर की पूजा करते थे, आखिर पूजा करते भी क्यों नहीं। डॉक्टर, जिंदगी की अंतिम सांस ले रहे व्यक्ति को फिर से स्वस्थ जो कर देते थे।
पहले डॉक्टरों में मरीज के प्रति सेवाभावना थी। मगर बदलते परिवेश में आज डॉक्टर, भगवान न रहकर व्यापारी बन गए हैं, जिन्हें मामूली जांच से लेकर गंभीर उपचार करने के लिए मरीजों से मोटी रकम चाहिए। पैसा लिए बिना डॉक्टर अब लाश का पोस्टमार्टम करने के लिए भी तैयार नहीं होते। वे परिजनों से सौदेबाजी करते हैं और तब तक मोलभाव होता है, जब तक पोस्टमार्टम की एवज में मोटी रकम न मिल जाए।
मुझे आज भी वह दिन याद है, जब छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर की पुरानी बस्ती निवासी एक गर्भवती महिला अपने पति के साथ गरीबी रेखा का राशन कार्ड लेकर इंदिरा गांधी जिला अस्पताल पहुंची। वहां मौजूद एक महिला चिकित्सक ने जांच करने के बाद आपरेशन करने की बात कहते हुए उस महिला के पति से 10 हजार की मांग की तथा उसे अपने निजी क्लीनिक में लेकर आने को कहा। तब महिला के पति ने रो-रोकर अपनी बदहाली की दास्तां सुनाई, लेकिन उस डॉक्टर का दिल तो पत्थर का था। उसने एक न सुनी और पैसे मिलने के बाद ही उपचार शुरू करने बात कही। इस चक्कर में काफी देरी हो गई और नवजात शिशु की दुनिया देखने से पहले ही अपनी मां के गर्भ में दम घुटकर मौत हो गयी।
डॉक्टरों की बनियागिरी यही खत्म होने वाली नहीं है। दो दिन पहले ही उसी अस्पताल में पदस्थ एक चिकित्सक ने पोस्टमार्टम के लिए मृतक के परिजनों से सौदेबाजी की। एक दशक के भीतर ऐसे कई मामले सामने आये हैं, जिनको याद करने के बाद डॉक्टर शब्द से घृणा होने लगती है। क्या सचमुच, बदलते परिवेश में डॉक्टर अब भगवान कहलाने के लायक नहीं रह गए हैं? क्या उन्हेंमरीज की जिंदगी से नहीं, बल्कि रूपए से प्यार है़? जी हां, अब डॉक्टरों में समर्पण की भावना नहीं रह गई है, इसीलिए वे मरीजों से लूट-खसोट करने लगे हैं। कई चिकित्सक तो फीस की शेष रकम लिए बिना परिजनों को मृतक की लाश भी नहीं उठाने देते।
हां, मगर कुछ चिकित्सक ऐसे भी है, जिन्होंने इस पेशे को आज भी गंगाजल की तरह पवित्र रखा हुआ है। वर्षों तक सरकारी अस्पताल में सेवा दे चुके अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. जी.के. नायक कहते हैं कि दर्द चाहे हड्डी का हो या किसी भी अंग में हो, कष्ट ही देता है। अस्थि के दर्द से तड़पता मरीज जब मेरे क्लीनिक में आता है तो मेरी पहली प्राथमिकता उसका दर्द दूर करने की होती है। दर्द से राहत मिलने पर मरीज के चेहरे पर जो सुकून नजर आता है, वह मेरे लिए अनमोल होता है।
हां, मगर कुछ चिकित्सक ऐसे भी है, जिन्होंने इस पेशे को आज भी गंगाजल की तरह पवित्र रखा हुआ है। वर्षों तक सरकारी अस्पताल में सेवा दे चुके अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. जी.के. नायक कहते हैं कि दर्द चाहे हड्डी का हो या किसी भी अंग में हो, कष्ट ही देता है। अस्थि के दर्द से तड़पता मरीज जब मेरे क्लीनिक में आता है तो मेरी पहली प्राथमिकता उसका दर्द दूर करने की होती है। दर्द से राहत मिलने पर मरीज के चेहरे पर जो सुकून नजर आता है, वह मेरे लिए अनमोल होता है।
स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ रश्मि सिंह कहती हैं कि मरीज का इलाज करते-करते हमारा उसके साथ एक अनजाना सा रिश्ता बन जाता है। मरीज हमारे इलाज से स्वस्थ हो जाए, तो उससे बेहतर बात हमारे लिए कोई नहीं हो सकती। मरीज अपने आपको डॉक्टर के हवाले कर देता है, उसे डॉक्टर पर पूरा भरोसा होता है। ऐसे में उसके इलाज और उसे बचाने की जिम्मेदारी डॉक्टर की होनी ही चाहिए।
डॉक्टरों द्वारा कथित तौर पर लापरवाही बरते जाने के बारे में बत्रा हॉस्पिटल के गुर्दा रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रीतपाल सिंह कहते हैं कि इलाज के दौरान किसी मरीज की तबियत ज्यादा बिगड़ने पर या उसकी मौत होने पर हमें भी पीड़ा होती है, लेकिन हम वहीं ठहर तो नहीं सकते। वह कहते हैं 'कोई भी डॉक्टर जान-बूझकर लापरवाही नहीं करता। हां, कभी-कभार चूक हो जाती है, लेकिन मैं मानता हूं कि डॉक्टर भी इंसान ही होते हैं, भगवान नहीं। डॉक्टर्स डे के बारे में डॉ. पी.के. नरूला कहते हैं अच्छी बात है कि एक दिन डॉक्टर के नाम है, लेकिन यह न भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि डॉक्टरों को किसी दिन विशेष से मतलब नहीं होता। वे हर दिन तन्मयता से अपना काम करते हैं।
खैर, राह से भटके चिकित्सकों को अपनी जिम्मेदारियों का अहसास आज भी हो जाए तो, इस पेशे को बदनाम होने से बचाया जा सकता है।
छत्तीसगढ़ के जांजगीर के राजेंद्र राठौर पत्रकारिता में 1999से जुड़े हैं और स्वतंत्र लेखन का शौक रखते हैं. लोगों तक अपनी बात पहुँचाने के लिए 'जन-वाणी' ब्लॉग लिखते है.




























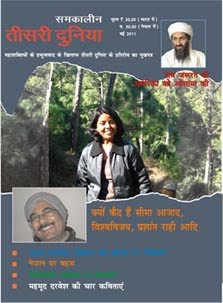



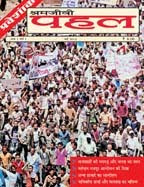



No comments:
Post a Comment